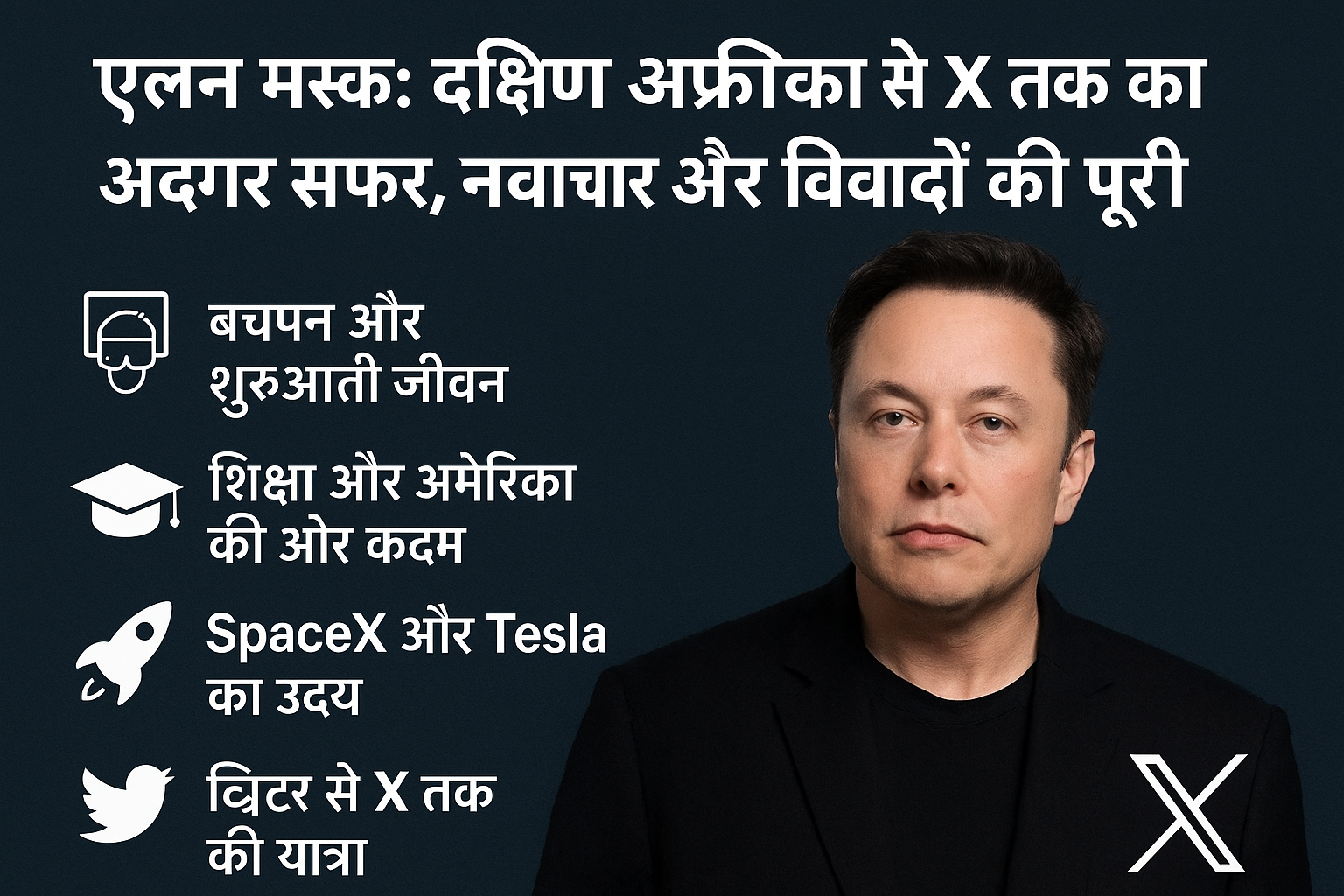लखनऊ/नई दिल्ली: जलवायु परिवर्तन आज दुनिया भर में सबसे बड़े संकटों में से एक है। वैज्ञानिकों के अनुसार, पिछले कुछ दशकों में मानव गतिविधियों के कारण धरती का तापमान तेजी से बढ़ा है। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हुई है, जैसे कि बाढ़, सूखा, ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र स्तर में वृद्धि। इन घटनाओं का गहरा असर भारत जैसे विकासशील देशों पर पड़ रहा है, जहां कृषि, उद्योग और जनसंख्या का बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर जलवायु के साथ जुड़ा हुआ है।
जलवायु परिवर्तन का भारत पर प्रभाव
भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इसके बावजूद, भारत जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े शिकारों में से एक है। यहां की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है, जो सीधे तौर पर जलवायु के अनुकूल है। हाल के वर्षों में बाढ़, सूखा, और अत्यधिक तापमान जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है।
जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव
भारत की कुल आबादी का लगभग 60% हिस्सा कृषि पर निर्भर है, जो जलवायु परिवर्तन के चलते सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत के कई हिस्सों में सूखा पड़ने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे फसल उत्पादन में कमी आई है। इसके विपरीत, मानसून के बदलते पैटर्न के कारण कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ और मिट्टी कटाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों पर प्रभाव
जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के जल संसाधन भी गंभीर संकट में हैं। देश के कई हिस्सों में भूजल स्तर तेजी से घट रहा है। इसके अलावा, हिमालयी ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों के जल प्रवाह में अनिश्चितता आ रही है। इससे भारत के कई राज्यों में जल संकट की स्थिति बन गई है।
विशेष रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्य अक्सर जल संकट का सामना करते हैं, जहां सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे न केवल कृषि प्रभावित होती है, बल्कि पेयजल की कमी भी लोगों के जीवन को मुश्किल बना रही है।
जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रभाव
जलवायु परिवर्तन का सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर भी हो रहा है। अत्यधिक तापमान के कारण हिट स्ट्रोक, श्वसन संबंधी समस्याएं और जलजनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। बाढ़ और सूखे की घटनाओं के बाद मच्छर जनित बीमारियों जैसे डेंगू और मलेरिया में वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के चलते फसल उत्पादन में कमी के कारण कुपोषण की समस्या भी बढ़ रही है।
समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव
जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसका सीधा असर भारत के तटीय क्षेत्रों पर पड़ रहा है। भारत की लंबी तटरेखा और बड़े तटीय शहर जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि समुद्र स्तर में वृद्धि से प्रभावित हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर जलवायु परिवर्तन की गति इसी तरह बनी रही, तो आने वाले दशकों में कई तटीय क्षेत्रों के जलमग्न होने का खतरा है।
1. तटीय शहरों पर खतरा
मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे वहां के लोगों को बाढ़ और तटीय क्षरण का सामना करना पड़ रहा है। इससे न केवल लोगों के घरों को खतरा है, बल्कि वहां के बुनियादी ढांचे को भी गंभीर क्षति हो रही है।
2. तटीय क्षेत्रों में आजीविका पर असर
भारत के कई तटीय क्षेत्रों में मछली पालन और कृषि प्रमुख आजीविका स्रोत हैं। समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण ये उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। मछलियों की प्रजातियों में कमी और खारे पानी का भूमि पर फैलाव कृषि को प्रभावित कर रहा है।
सरकार और नीतिगत प्रतिक्रियाएं
1. भारत सरकार की नीतियां
जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। भारत ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर कर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में शामिल होने का संकल्प लिया है। इसके तहत भारत ने 2030 तक अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 33% तक की कमी करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही, सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं।
2. नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान
भारत में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन” (International Solar Alliance) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटना है। इसके अलावा, भारत के कई राज्यों में ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए नीतिगत सुधार किए जा रहे हैं।
समाज की भूमिका और जागरूकता
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार के साथ-साथ समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कई गैर-सरकारी संगठन और पर्यावरणविद सक्रिय हैं।
1. व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास
लोगों को अपने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलाव करने की आवश्यकता है, जैसे कि प्लास्टिक का कम उपयोग, ऊर्जा की बचत, और जल संरक्षण। इसके अलावा, हरित ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और वृक्षारोपण जैसे उपाय भी जलवायु परिवर्तन से निपटने में मददगार हो सकते हैं।
2. शैक्षणिक संस्थानों और युवाओं की भूमिका
युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में जलवायु शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है। इससे अगली पीढ़ी जलवायु संकट को बेहतर तरीके से समझ सकेगी और इसके समाधान के लिए तैयार हो सकेगी।
भारत का भविष्य और जलवायु परिवर्तन
जलवायु परिवर्तन से लड़ना न केवल सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि समाज और व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयासों की आवश्यकता है। यदि हम अभी ठोस कदम नहीं उठाते हैं, तो भारत जैसे देश को आने वाले दशकों में गंभीर पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमें तत्काल ठोस नीतिगत सुधारों, तकनीकी विकास, और सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता है।